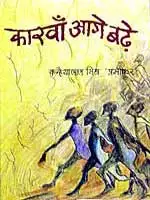|
कहानी संग्रह >> कारवाँ आगे बढ़े कारवाँ आगे बढ़ेकन्हैयालाल मिश्र
|
345 पाठक हैं |
|||||||
हिन्दी के यशस्वी गद्य लेखक, शैलीकार एवं पत्रकार की कलम से संस्मरणात्मक निबन्धों का संकलन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
राष्ट्रीय चरित्र पर ऐसी पुस्तक सम्भवतः देश की किसी भी
भाषा के पास नहीं है। नयी पीढ़ी के हाथों में पहुँचकर तो यह मशाल का काम
कर सकती है। ये अछूते प्रेरक निबन्ध उस लेखनी के धनी, प्रथम श्रेणी के
साहित्यकार-पत्रकार की अमूल्य देन हैं जिसे ‘शैलीकारों का
शैलीकार’ कहा जाता है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में-
‘‘इन संस्मरणात्मक निबन्धों में प्रचारक की हुंकार नहीं, सन्मित्र की पुचकार है, जो पाठक का कन्धा थपथपाकर उसे चिन्तन की राह पर ले जाती है। वह सड़कों पर, स्टेशनों पर, दफ़्दरों में, घरों में, कहें पूरे राष्ट्रीय जीवन की कुरूपता देखता है-मैं इस कुरूपता से बचूँगा और दूसरे नागरिकों को भी बचाऊँगा। प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए नागरिकों का कारवाँ तैयार हो जाता है। हर पन्ना उस कारवाँ के लिए हरी झण्डी है।’’
हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक जिसके भी हाथ में जाएगी वह इसे आगे बढ़ाएगा और यह देश के कोने-कोने में पहुँचकर आलोक विकीर्ण करेगी।
अपनी जन्मभूमि देवबन्द को-
1. जिसकी ममतामयी मिट्टी में पल-खेलकर मैं बड़ा हुआ,
2. जिसके भ्रातृमण्डल पुस्तकालय में बैठकर मैंने पाठ्यक्रम की तरह सरस्वती, माधुरी, चाँद, सुधा आदि पत्रों और चन्द्रकान्ता सन्तति से प्रेमाश्रम तक के विषयक्षेत्र में फैले उपन्यासों, कहानियों, इतिहास-ग्रन्थों और वैचारिक ग्रन्थों को पढ़, स्कूली शिक्षा के अभाव में भी जीवन के व्यापक क्षितिज को आत्मसात किया,
3. जहाँ मेरे जीवन में नागरिकता, सामाजिकता, मानव-निष्ठा, साहित्य-सर्जना एवं पत्रकारिता के अंकुर फूटे और अन्धश्रद्धा की जड़ता के आत्मघाती बन्धन टूटे,
4. जहाँ मैंने गाँधीजी की छाया में अपनी मातृभूमि भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष-यज्ञ में अपने पारिवारिक मोह की आहुति दे जीवन की कृतार्थता का अनुभव किया,
5. जिसे राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश और भारत की प्रथम पार्लियामेण्टेरियन महिला श्रीमती लेखवती जैन की जन्मभूमि और भारतीय जैन समाज में विचार-क्रान्ति के प्रथम पुरोधा बाबू सूरजभान वकील, क्रान्तिकारी शेखुलहिन्द, मौ. महमूदुल हसन एवं शेखुल इस्लाम, मौ. हुसैन अहमदमदनी की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है,
-यह कृति सादर समर्पित।
‘‘इन संस्मरणात्मक निबन्धों में प्रचारक की हुंकार नहीं, सन्मित्र की पुचकार है, जो पाठक का कन्धा थपथपाकर उसे चिन्तन की राह पर ले जाती है। वह सड़कों पर, स्टेशनों पर, दफ़्दरों में, घरों में, कहें पूरे राष्ट्रीय जीवन की कुरूपता देखता है-मैं इस कुरूपता से बचूँगा और दूसरे नागरिकों को भी बचाऊँगा। प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए नागरिकों का कारवाँ तैयार हो जाता है। हर पन्ना उस कारवाँ के लिए हरी झण्डी है।’’
हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक जिसके भी हाथ में जाएगी वह इसे आगे बढ़ाएगा और यह देश के कोने-कोने में पहुँचकर आलोक विकीर्ण करेगी।
अपनी जन्मभूमि देवबन्द को-
1. जिसकी ममतामयी मिट्टी में पल-खेलकर मैं बड़ा हुआ,
2. जिसके भ्रातृमण्डल पुस्तकालय में बैठकर मैंने पाठ्यक्रम की तरह सरस्वती, माधुरी, चाँद, सुधा आदि पत्रों और चन्द्रकान्ता सन्तति से प्रेमाश्रम तक के विषयक्षेत्र में फैले उपन्यासों, कहानियों, इतिहास-ग्रन्थों और वैचारिक ग्रन्थों को पढ़, स्कूली शिक्षा के अभाव में भी जीवन के व्यापक क्षितिज को आत्मसात किया,
3. जहाँ मेरे जीवन में नागरिकता, सामाजिकता, मानव-निष्ठा, साहित्य-सर्जना एवं पत्रकारिता के अंकुर फूटे और अन्धश्रद्धा की जड़ता के आत्मघाती बन्धन टूटे,
4. जहाँ मैंने गाँधीजी की छाया में अपनी मातृभूमि भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष-यज्ञ में अपने पारिवारिक मोह की आहुति दे जीवन की कृतार्थता का अनुभव किया,
5. जिसे राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश और भारत की प्रथम पार्लियामेण्टेरियन महिला श्रीमती लेखवती जैन की जन्मभूमि और भारतीय जैन समाज में विचार-क्रान्ति के प्रथम पुरोधा बाबू सूरजभान वकील, क्रान्तिकारी शेखुलहिन्द, मौ. महमूदुल हसन एवं शेखुल इस्लाम, मौ. हुसैन अहमदमदनी की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है,
-यह कृति सादर समर्पित।
-क. ला. प्रभाकर
अगले पन्नों में
भारत के एक नागरिक विदेश गये। एक बार वे
यूरोप के किसी देश
में रेल से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों पैर बूट सहित सामने की
सीट पर रख लिये। उनके लिए एक साधारण बात थी; क्योंकि हमारे देश में
पढ़े-अनपढ़े सभी ऐसा करते हैं।
उनके पास ही बैठे थे एक बूढ़े सज्जन। उन्होंने अपने ओवरकोट की जेब से पुराने अख़बार का साफ़ कटा-छँटा एक टुकड़ा निकाला और भारत के नागरिक से कहा-‘‘कृपा कर ज़रा अपने पैर उठाइए।’’
इन्होंने पैर उठाये, तो उन्होंने पैरों की जगह वह काग़ज़ रख दिया और नम्रता से कहा-‘‘अब आप पैर रख लीजिए इस तरह आपके आराम में ख़लल नहीं पड़ेगा और मेरे देश की यह चीज़-सीट की गद्दी-भी ख़राब नहीं होगी।’’
धन्यवाद देकर भारत के नागरिक ने कागज पर पैर रख लिये। थोड़ी देर बार बूढ़े सज्जन ने अपनी टोकरी से केले निकाले, छीलकर खाये और उनके छिलकों को वैसै ही एक काग़ज़ में लपेटकर जेब में रख लिया।
भारत के नागरिक से न रहा गया और पूछ ही लिया-‘‘बुजुर्गवार, ये छिलके आपने जेब में क्यों रख लिये हैं ?’’ उत्तर मिला-‘‘यहाँ इन्हें मैं कहाँ डालता ! अब स्टेशन पर उतरकर इन्हें कूड़ेदान में डाल दूँगा।’’
एक होता है नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है नागरिक का राष्ट्रीय चरित्र। वह बूढ़ा राष्ट्रीय चरित्र का कितना उत्तम नमूना था कि उसे अपने देश की हरेक चीज़ की सुरक्षा का भी ध्यान था और सफ़ाई-स्वच्छता का भी।
भारत के एक नागरिक, जो उम्र में जवान थे और फ़ैशन में पैरिस किसी स्टेशन से लखनऊ के लिए रेल में बैठे। दो सीटों के बीच, दीवार से सटाकर, क़ुली ने उनका होल्डॉल खड़ा कर दिया। पास ही वे बैठ गये। फ़ैशन साहबी, पर आदत नवाबी ! हर घण्टे पान खायें और पान भी तम्बाक़ू वाला। अब हालत यह कि सामने की सीट पर दोनों पैर रखे, वे पसरे हैं और जहाँ दूसरे मुसाफ़िर पैर रखते हैं, वहाँ पान की लुआबदार पीक थूके जा रहे हैं।
यह आ गया लखनऊ, वे कूदकर प्लेटफ़ॉर्म पर आ गये। उनके इशारे पर कुली ने उनका बिस्तर छुआ, तो बोझ ज़्यादा। उसने झटके के साथ बिस्तर को दोनों सीटों के बीच, नीचे के तख़्ते पर डाला और घसीटकर दरवाजे पर ले आया। उस बेचारे को क्या पता कि यहाँ पान की पीक का परनाला बह रहा है, पर बिस्तर उस परनाले के उपर से आया, तो पीक उसे प्यारे दोस्त की तरह लिपट गयी। साहब का नया होल्डॉल अब एकदम रंगीन, जैसे किसी सीखतड़ ने उस पर पेण्टिंग का अभ्यास किया हो।
साहब ने प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े-खड़े यह देखा तो झल्ला पड़े-‘‘अबे, तू बड़ा बेवकूफ है।’’ उसी सीट पर एक मसख़रे सज्जन बैठे थे। खिड़की से बाहर झाँककर बोले-‘‘साहब बहादुर, यह क़ुली बड़ा नहीं, छोटा बेवकूफ़ है। बड़ा बेवकूफ़ तो वह था, जो कुली के आने से पहले इस डब्बे में थूक गया।’’ कटकर रह गये बेचारे !
एक होता है कि नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है उसका राष्ट्रीय चरित्र। यह साहब बहादुर राष्ट्रीय चरित्र का कितना घटिया नमूना थे कि अपने देश की चीज़ों की सुरक्षा का भाव तो उनमें कहाँ होता, जब उन्हें स्वच्छ-साफ़ रखने की भावना भी उनमें नहीं थी।
1948 में मुझे तीसरी बार प्लूरिसी हुई। मैं चिकित्सा और विश्राम के लिए कुछ महीने मसूरी रहा। उन्हीं दिनों की डायरी के दो पन्ने यहाँ प्रस्तुत हैं।
डिपो मसूरी की सबसे ऊँची चोटी है। देखने लायक़ तो वहाँ कुछ नहीं है, पर है वह रहने लायक़ जगह। शहरों में ऐसी ताज़ी और महकती हवा कहाँ ? आज हम उधर को चढ़ चले। थका देने वाली चढ़ाई थी। थक गये, पर पहाड़ी चढ़ाई की थकान कि चढ़े भी जल्दी और उतरे भी जल्दी।
आओ कुछ देर सुस्ताएँ। प्रस्ताव किसी का हो, समर्थन सबका इसे मिला, पर बैठें कहाँ ? नगरपालिका ने स्थान-स्थान पर सीमेण्ट की बेंचें डाल रखी हैं। किसी आते जाते ने बताया-‘‘अगले मोड़ पर ही बेंच है और वहाँ का दृश्य भी सुन्दर है।’’ आशा धीरज की जननी है, हम लोग आगे बढ़े। वह सामने मोड़ और मोड़ के सामने ढलते सूर्य की किरणें बादलों की पेण्टिंग बनाने मैं तल्लीन; यह ब्रुश मारा और वह ब्रुश मारा। यह बना बैल और वह मिटा घोड़ा !
चलो बेंच पर बैठकर देखेंगे यह दृश्य और खाएँगे ताज़ी हवा, मन ने एक फुरैरी ली कि पिण्डलियों ने लम्बे डग भरे। वह दीख रही है बेंच; पगडण्डी से एक ओर बचा, एक बड़ा-सा शिलाखण्ड और उस पर रखी लम्बी बेंच। सामने दूर-दूर तक फैली विशाल पर्वतमालाएँ और ठीक नीचे हज़ारों फ़ीट गहरा खड्ड; हमारे जीवन की तरह, जिसमें शिव और शैतान का एक साथ निवास है। सोचा, नगरपालिका का इंजीनियर भी सम्भवतः कवि है तभी तो क्या बढ़िया जगह चुनी है उसने बेंच रखने के लिए !
दो लम्बी कुलाँचें और मैं अब बेंच के पास। मेरे दोनों हाथ बेंच की पीठ पर और मेरी खुली आँखों में बादलों के बनते-बिगड़ते चित्र। मैं भावना की मधुर पुलक में आनन्द-विभोर हुआ जा रहा हूँ कि तभी आया हवा का एक हलका झोंका और मेरी नाक पर मारा किसी ने तेज़ चाकू। नाक तो नहीं कटी, पर दिमाग़ भिन्ना गया। यह चाकू ख़ून करने वाला लोहे के फलक का चाकू न था, पेशाब की तेज़ दुर्गन्ध का चाकू था। बेंच की आड़ का लाभ उठाकर स्वतन्त्र भारत के नागरिक नर-नारियों ने इस स्थान का उपयोग किया था।
कुत्ते भी स्थान देखकर ही पेशाब करते हैं, पर उन नर-नारियों ने बिना स्थान देखे ही अपनी जरूरत पूरी की थी; क्योंकि इस बेंच से थोड़ी दूर पर ही सरकारी पेशाबघर था। मेरी इच्छा हुई कि मैं पूरे ज़ोर से रो पड़ूँ।
मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी और सामने ही सरकारी पेशाबघर था। मैं उधर मुड़ा, पर दरवाज़े तक अभी पहुँचा-न-पहुँचा कि तेज़ दुर्गन्ध का एक झोंका भीतर से आया। मसूरी की नगरपालिका इन दिनों सरकारी प्रबन्धक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) के हाथों में थी और मैं उनकी सफ़ाई-व्यवस्था का प्रशंसक था, पर इस झोंके की पहली ही झोंक में निन्दा का नशा मुझ पर छा गया-‘जाने कब से इस पेशाबघर में पानी की बूँद नहीं पड़ी। मज़ा आ जाए, अगर एक रात के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब को इसमें बन्द कर दिया जाए !’’
ज़रा आगे बढ़कर मैंने देखा कि भीतर पाँच मनुष्यों के लिए स्थान है और पाँचों स्थानों पर पाँच पढ़े-लिखे-सज्जन खड़े हैं। मैं बाहर लौटने को ही था कि देखा दूसरे पेशाबघरों की तरह यह भी प्रवाही (फ़्लश सिस्टम वाला) है और तीसरे स्थान के ऊपर वह साफ़ लगी है पानी की टंकी, जिसमें लटक रही है ज़ंजीर। इसमें नीचे एक छोटा कड़ा भी है कि उसमें दो उँगली डालें और दें ज़रा-सा झटका कि बस पाँचों स्थानों में बह जाए पानी ही पानी और दुर्गन्ध ऐसी भागे कि जैसे घरवालों के जागने पर चोर भागे।
मेरे पैर ठिठक गये। मैंने देखा, वे पाँचों सज्जन रूमालों से अपनी नाक दबाये खड़े हैं। क्या टंकी ख़राब है ? मेरे मन में नया प्रश्न उपजा कि मैंने आगे बढ़कर कड़े के द्वारा ज़ंजीर को ज़ोर का झटका दिया। पाँचों स्थानों के नल बादल की तरह बरस पड़े।
वे बरसे, मैं बाहर आया। मेरे पीछे ही पीछे एक दाढ़ी वाले सज्जन बाहर आये। उनकी पतलून के पाँवचे नीचे से भीग गये थे और बूटों में पानी आ गया था। मुझे उन्होंने कड़वी आँखों से घूरा कि इतने में वे चारों भी भीतर से बाहर आ गये। छींटे तो सभी पर तकड़े पड़े थे, पर शायद दाढ़ी वाले सज्जन दीवार से कुछ ज़्यादा सटकर खड़े थे, इसलिए उनकी पतलून पूरी तरह रसवर्षिणी हो गयी थी।
तमककर बोले-‘‘क्यों जी, यह आपने क्या हिमाक़त की ?’’ मैं इस समय स्वयं लड़ने की नहीं, तीतर लड़ाने की मूड में था। मुसकराकर मैंने कहा-‘‘हिमाक़त ? वह तो आपकी जान बचाने की हिकमत थी जनाब !’’
ग़ुर्राकर बोले-‘‘जान बचाने की कैसी हिकमत ?’’
मैंने अपने गले को पूरी तरह ठण्डा कर एक तेज़ आलपीन चुभाया-‘‘आप नाक को इतनी ज़ोर से दबा रहे थे कि मुझे आपका दम घुटने का ख़तरा दिखाई दिया; और भाई जी, यह तो बकरे भी जानते हैं कि दम घुटने से जान चली जाती है।’’
एक दूसरे साहब बीच में टमक पड़े-‘‘फिर आपको ज़ंजीर ही खींचनी थी, तो धीरे से खींचते। आपने तो ऐसा झटका मारा कि जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी हो।’’
बुजुर्गाना लहजे में मैंने कहा-‘‘हाँ, जी, मैंने यही समझा कि आप बड़ी मुसीबत में हैं।’’
वे समझ गये कि इस पत्थर पर जोंक नहीं लग सकती और खिसके। अपनी भीगी पतलून को एक झटका देते हुए वे सज्जन बोले-‘‘ऐसे-ऐसे जाहिल भी मसूरी आ जाते हैं.’’ मैंने उनकी व्यंग्य कविता को संगीत के जाहिल भी मसूरी आ जाते हैं।’’ मैंने उनकी व्यंग्य कविता को संगीत के स्वर में चढ़ाते हुए कहा-‘‘जी हाँ, यही तो बात है कि ऐसे-ऐसे जाहिल भी मसूरी आ जाते हैं कि बदबू में मरते रहते हैं, पर ज़ंजीर नहीं खींचते।’’
दिमाग़ में जोशीले लड़कपन का जो उबाल आया था, वह उतर गया, तो एक हलकी उदासी मुझ पर छा गयी-यों ही मैं उन बेचारों से उलझा; उनका या किन्ही दूसरों का इसमें कुछ भी दोष नहीं। उनसे पहले जाने कितने नागरिक आ चुके होंगे। वे सभी दुर्गन्ध के स्रष्टा थे, पर सभी उसके शिकार भी।
एक होता है नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है नागरिक का राष्टीय चरित्र। बेंच की आड़ में पेशाब करने वाले नर-नारी, नागरिक के चरित्र की दृष्टि से और राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से भी बुरे-से-बुरा नमूना थे; क्योंकि उनमें उचित स्थान देखकर ज़रूरत पूरी करने की नागरिक शालीनता भी नहीं थी और राष्ट्र के स्वच्छ-सुन्दर स्थानों को स्वच्छ-सुन्दर रखने की उदात्त राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था।
और सरकारी पेशाबघर के वे पाँच सज्जन ? वे कर्महीन थे, जिनमें राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाने की भी वृति नहीं थी, राष्ट्र को अपनी ओर से सुविधा देने की तो बात ही दूर। वे दो पैर के पशु थे, जो डण्डे से हँकते हैं, स्वयं सोच-विचारकर नहीं चलते।
प्रिंस क्रोपाटकिन का रूस के नये इतिहास में वही स्थान है, जो भारत को नये इतिहास में लोकमान्य तिलक का। रूस ज़ारशाही से मुक्त हो गया था और लेनिन महान् रूस की समाज-व्यवस्था को समाजवादी रूप देने में जुटे हुए थे। रूस के नागरिकों को नपा-तुला भोजन मिलता था और पूरे देश के दूध का पनीर बनाकर विदेशों को भेजा जाता था, जिसके बदले में मशीनें ख़रीदी जाती थीं। रूस के नागरिक दूध से वंचित थे। एक दिन लेनिन प्रिंस क्रोपाटनिक से मिलने गये। उनकी कमजोरी और बुढ़ापा देखकर लेनिन ने कहा-‘‘मैं आपके लिए एक गाय भेजने की विशेष व्यवस्था करता हूँ।’’
प्रिंस क्रोपाटकिन ने कहा-‘‘मैं भी रूस का एक नागरिक हूँ, इसलिए मैं अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं चाहता।’’ और कुछ दिन बाद प्रिंस क्रोपाटकिन की मृत्यु हो गयी।
दूसरे महायुद्ध के बाद जापान में भी राशनिंग करना पड़ा। सब नागरिकों को नपा-तुला अन्न मिलता था। एक रिटायर्ड जनरल की ख़ुराक ज़्यादा थी। राशनिंग में मिलने वाला अन्न कम पड़ता था, वे भूखे रह जाते थे। पास-पड़ोसियों ने उनसे कहा कि सरदार से ज़्यादा अन्न देने की प्रार्थना करें, पर उनका उत्तर था-‘‘युद्ध के कारण देश में अन्न की कमी है। सरकार व्यवस्था को सँभाल रही है, मैं सरकार का काम बढ़ाना नहीं चाहता। दूसरे नागरिक भी बहुत-सी दिक़्कतें बरदाश्त कर रहे हैं। मैं भी सबके साथ रहूँगा।’’ और रोज़-रोज़ की भूख से धीरे-धीरे उनकी मृत्यु हो गयी।
दूसरे महायुद्ध के बाद की ही बात है। इंग्लैण्ड टूटा-फूटा पड़ा था, हर चीज़ की कमी थी। भारत की अन्तरिम सरकार (1946-47) के मन्त्री जगजीवन राम जी किसी सम्मेलन में लन्दन गये। वहाँ की सरकार ने इधर-उधर जाने-आने के लिए एक टैक्सी दी और प्रेट्रोल के कूपन की एक कॉपी भी। पेट्रोल पर कण्ट्रोल था, पर इस सरकारी कूपन से कहीं भी, कितना भी लिया जा सकता था।
सम्मेलन के बाद मन्त्री जी जब भारत लौटने लगे, तो उस कॉपी में पाँच कूपन बाक़ी थे। टैक्सी के ड्राइवर से उन्होंने कहा-‘‘लो, ये कूपन तुम ले लो, तुम्हें इनसे लाभ होगा। अपनी टैक्सी के लिए पेट्रोल ले लेना।’’
मन्त्री जी का ख़याल था कि टैक्सी-ड्राइवर इससे ख़ुश होगा, उन्हें झुककर सलाम करेगा, पर वह तो सुनते ही गुस्से से भर गया-‘‘आप मुझे बेईमान समझते हैं ? मैं आपकी राय में गद्दार हूँ कि अपनी सरकार को धोखा देकर अपने लिए नियत भाग से अधिक पेट्रोल ले लूँगा ? आपके देश में ऐसे ही नागरिक होते हैं ? आप ये कूपन अपने स्वागत-अधिकारी को लौटाएँ; मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ ?’’
एक होता है नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है नागरिक का राष्ट्रीय चरित्र। प्रिंस क्रोपाटकिन, जापानी जनरल और इंग्लैण्ड का ड्राइवर नागरिक के अपने और राष्ट्रीय चरित्र के उत्तम नमूने हैं। इसी श्रृंखला में ही जगजीवन राम का ही दूसरा संस्मरण है उसी यात्रा का। वे घुटनों में दर्द के कारण नाश्ते में अण्डा लेते हैं, पर द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन बम्बार्डमेण्ड से इंग्लैण्ड के मुर्ग़ीख़ाने क्षत-विक्षत हो गये थे, लन्दन में अण्डे पर कण्ट्रोल था; डॉक्टर के लिखने पर ही किसी को अण्डे मिलते थे। स्वागत-अधिकारी तीन दिन प्रयत्न करने पर भी जगजीवनराम जी को अण्डा नहीं दे सका। अन्त में उसने क्षमा-याचना की, तो जगजीवनराम जी ने पूछा-‘‘हाँ, आरम्भ में एक बार हुआ था। बात यह हुई कि डॉक्टर ने एक ग़रीब बीमार को दो दिन के लिए चार-चार अण्डे लिखे। वह मुर्ग़ीख़ाने से आठ अण्डे ले आया और अपने अमीर परिचित के हाथ काफ़ी ऊँचे मूल्य पर उन्हें बेच दिया। पता चलने पर पड़ोसियों ने इकट्ठे होकर उसका घर घेर लिया और उसकी इतनी निन्दा की कि उसे मुहल्ला छोड़कर भागना पड़ा, बस फिर कभी ऐसा नहीं हुआ।’’
आँख खोल देने वाले संस्मरण हैं ये और इनका सन्देश है कि यदि देश में किसी-किन्हीं चीज़ों की कमी हो, तो अच्छे चरित्र के नागरिक उसे धीरज से सहते हैं; सरकार को, समाज को अच्छी परिस्थितियाँ पैदा करने में सहयोग देते हैं, हुल्लड़ मचाकर, भ्रष्टाचार फैलाकर अव्यवस्था नहीं बढ़ाते। यही नहीं, यदि कोई चरित्रहीन नागरिक अपनी सुविधा या स्वार्थ के लिए अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करता है, तो राष्ट्रीय चरित्र के नागरिक सामूहिक रूप में उनका निन्दात्मक प्रतिवाद कर अव्यवस्था को असम्भव बना देते हैं।
राष्ट्रीय चरित्र अनुशासन से बनता है और अनुशासन की जड़ें नागरिकों के मन में जमती हैं राजदण्ड के भय से। धर्म भावना या प्रशिक्षण अनुशासन को सहज बनाकर उसे नागरिकों का स्वभाव-संस्कार बना देते हैं; इसे ही कहते हैं आत्मानुशासन। इस स्थिति में दण्ड-भय की कम-से-कम आवश्यकता रह जाती है। बीसवीं सदी के तीसरे दशक की बात है। हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में वरिष्ठ प्राध्यापक श्री गाँधी ने वार्षिक परीक्षा का प्रश्नपत्र तैयार किया और अपनी मेज़ के दराज़ में रख दिया। उनके पुत्र ने, जो उसी श्रेणी का छात्र था, वह पढ़ लिया और अपने दो मित्र-छात्रों को भी बता दिया। प्राध्यापक गाँधी को कुछ पता न चला। परीक्षा का परिणाम निकला, तो बेटे को 85 प्रतिशत अंक मिले।
वे चौंके, पुत्र से पूछा-‘‘तुम्हारे इतने नम्बर कैसे आये, सच बताओ !’’
बेटे ने बाप को रद्दा दिया-‘‘पापा, मैं रात में एक-एक बजे उठकर सुबह तक पढ़ा हूँ !’’ गाँधी अपने में स्पष्ट थे-‘‘वह सब मुझे मालूम है, तुम्हारे 65 प्रतिशत से अधिक नम्बर नहीं आ सकते; सच बताओ; नहीं तो भोजन नहीं करूँगा।’’ पुत्र ने स्वीकारा कि उसने प्रश्नपत्र देख लिया था और अपने दो साथियों को भी बताया है। प्रोफ़ेसर गाँधी ने उन साथियों के नाम नहीं पूछे और उसी दिन कुलपति पण्डित मदनमोहन मालवीय से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र का दो वर्ष के लिए वे ‘रस्टीकेशन’ (परीक्षा देने के अधिकार से वंचित) कर दें।
मालवीय जी बहुत दयालु थे। उन्होंने गाँधी को समझाया-‘‘प्रथम श्रेणी तो उसकी निश्चित थी ही, फिर उसने प्रश्नपत्र को बेचा नहीं, अपने दो मित्रों को ही बताया। अब यह रहने दो, बालक का भविष्य गड़बड़ा जाएगा।’’ गाँधी का उत्तर सदा स्मरणीय था-‘‘महाराज, मैं चुप रह जाऊँगा, तो हमारे विश्वविद्यालय की महिमा घटेगी’’ और वे आदेश पर हस्ताक्षर कराने के बाद ही उठे। प्रोफ़ेसर गाँधी आत्मानुशासन के उत्तम उदाहरण हैं। गाँधी जी अपने अहिंसात्मक युद्ध के द्वारा देश के जनमानस को आत्मानुशासन का सामूहिक प्रशिक्षण दे रहे थे, पर वह प्रक्रिया उनके बाद आगे नहीं बढ़ी। नागरिकों के लिए इसी प्रशिक्षण के निबन्धपुष्प खिले हैं अगले पन्नों में। इन संस्मरणात्मक निबन्धों में प्रचारक की हुंकार नहीं, सन्मित्र की पुचकार है, जो पाठक का कन्धा थपथपाकर उसे चिन्तन की राह पर ले आती है। वह सड़कों पर, स्टेशनों पर, दफ़्तरों में, घरों में ! कहें पूरे राष्टीय जीवन में कुरूपता देखता है और संकल्प करता है-मैं इस कुरूपता से बचूँगा और दूसरे नागरिकों को भी बचाऊँगा। बस प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए नागरिकों का कारवाँ तैयार हो जाता है। आगे का हर पन्ना उस कारवाँ के लिए हरी झण्डी है।
उनके पास ही बैठे थे एक बूढ़े सज्जन। उन्होंने अपने ओवरकोट की जेब से पुराने अख़बार का साफ़ कटा-छँटा एक टुकड़ा निकाला और भारत के नागरिक से कहा-‘‘कृपा कर ज़रा अपने पैर उठाइए।’’
इन्होंने पैर उठाये, तो उन्होंने पैरों की जगह वह काग़ज़ रख दिया और नम्रता से कहा-‘‘अब आप पैर रख लीजिए इस तरह आपके आराम में ख़लल नहीं पड़ेगा और मेरे देश की यह चीज़-सीट की गद्दी-भी ख़राब नहीं होगी।’’
धन्यवाद देकर भारत के नागरिक ने कागज पर पैर रख लिये। थोड़ी देर बार बूढ़े सज्जन ने अपनी टोकरी से केले निकाले, छीलकर खाये और उनके छिलकों को वैसै ही एक काग़ज़ में लपेटकर जेब में रख लिया।
भारत के नागरिक से न रहा गया और पूछ ही लिया-‘‘बुजुर्गवार, ये छिलके आपने जेब में क्यों रख लिये हैं ?’’ उत्तर मिला-‘‘यहाँ इन्हें मैं कहाँ डालता ! अब स्टेशन पर उतरकर इन्हें कूड़ेदान में डाल दूँगा।’’
एक होता है नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है नागरिक का राष्ट्रीय चरित्र। वह बूढ़ा राष्ट्रीय चरित्र का कितना उत्तम नमूना था कि उसे अपने देश की हरेक चीज़ की सुरक्षा का भी ध्यान था और सफ़ाई-स्वच्छता का भी।
भारत के एक नागरिक, जो उम्र में जवान थे और फ़ैशन में पैरिस किसी स्टेशन से लखनऊ के लिए रेल में बैठे। दो सीटों के बीच, दीवार से सटाकर, क़ुली ने उनका होल्डॉल खड़ा कर दिया। पास ही वे बैठ गये। फ़ैशन साहबी, पर आदत नवाबी ! हर घण्टे पान खायें और पान भी तम्बाक़ू वाला। अब हालत यह कि सामने की सीट पर दोनों पैर रखे, वे पसरे हैं और जहाँ दूसरे मुसाफ़िर पैर रखते हैं, वहाँ पान की लुआबदार पीक थूके जा रहे हैं।
यह आ गया लखनऊ, वे कूदकर प्लेटफ़ॉर्म पर आ गये। उनके इशारे पर कुली ने उनका बिस्तर छुआ, तो बोझ ज़्यादा। उसने झटके के साथ बिस्तर को दोनों सीटों के बीच, नीचे के तख़्ते पर डाला और घसीटकर दरवाजे पर ले आया। उस बेचारे को क्या पता कि यहाँ पान की पीक का परनाला बह रहा है, पर बिस्तर उस परनाले के उपर से आया, तो पीक उसे प्यारे दोस्त की तरह लिपट गयी। साहब का नया होल्डॉल अब एकदम रंगीन, जैसे किसी सीखतड़ ने उस पर पेण्टिंग का अभ्यास किया हो।
साहब ने प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े-खड़े यह देखा तो झल्ला पड़े-‘‘अबे, तू बड़ा बेवकूफ है।’’ उसी सीट पर एक मसख़रे सज्जन बैठे थे। खिड़की से बाहर झाँककर बोले-‘‘साहब बहादुर, यह क़ुली बड़ा नहीं, छोटा बेवकूफ़ है। बड़ा बेवकूफ़ तो वह था, जो कुली के आने से पहले इस डब्बे में थूक गया।’’ कटकर रह गये बेचारे !
एक होता है कि नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है उसका राष्ट्रीय चरित्र। यह साहब बहादुर राष्ट्रीय चरित्र का कितना घटिया नमूना थे कि अपने देश की चीज़ों की सुरक्षा का भाव तो उनमें कहाँ होता, जब उन्हें स्वच्छ-साफ़ रखने की भावना भी उनमें नहीं थी।
1948 में मुझे तीसरी बार प्लूरिसी हुई। मैं चिकित्सा और विश्राम के लिए कुछ महीने मसूरी रहा। उन्हीं दिनों की डायरी के दो पन्ने यहाँ प्रस्तुत हैं।
डिपो मसूरी की सबसे ऊँची चोटी है। देखने लायक़ तो वहाँ कुछ नहीं है, पर है वह रहने लायक़ जगह। शहरों में ऐसी ताज़ी और महकती हवा कहाँ ? आज हम उधर को चढ़ चले। थका देने वाली चढ़ाई थी। थक गये, पर पहाड़ी चढ़ाई की थकान कि चढ़े भी जल्दी और उतरे भी जल्दी।
आओ कुछ देर सुस्ताएँ। प्रस्ताव किसी का हो, समर्थन सबका इसे मिला, पर बैठें कहाँ ? नगरपालिका ने स्थान-स्थान पर सीमेण्ट की बेंचें डाल रखी हैं। किसी आते जाते ने बताया-‘‘अगले मोड़ पर ही बेंच है और वहाँ का दृश्य भी सुन्दर है।’’ आशा धीरज की जननी है, हम लोग आगे बढ़े। वह सामने मोड़ और मोड़ के सामने ढलते सूर्य की किरणें बादलों की पेण्टिंग बनाने मैं तल्लीन; यह ब्रुश मारा और वह ब्रुश मारा। यह बना बैल और वह मिटा घोड़ा !
चलो बेंच पर बैठकर देखेंगे यह दृश्य और खाएँगे ताज़ी हवा, मन ने एक फुरैरी ली कि पिण्डलियों ने लम्बे डग भरे। वह दीख रही है बेंच; पगडण्डी से एक ओर बचा, एक बड़ा-सा शिलाखण्ड और उस पर रखी लम्बी बेंच। सामने दूर-दूर तक फैली विशाल पर्वतमालाएँ और ठीक नीचे हज़ारों फ़ीट गहरा खड्ड; हमारे जीवन की तरह, जिसमें शिव और शैतान का एक साथ निवास है। सोचा, नगरपालिका का इंजीनियर भी सम्भवतः कवि है तभी तो क्या बढ़िया जगह चुनी है उसने बेंच रखने के लिए !
दो लम्बी कुलाँचें और मैं अब बेंच के पास। मेरे दोनों हाथ बेंच की पीठ पर और मेरी खुली आँखों में बादलों के बनते-बिगड़ते चित्र। मैं भावना की मधुर पुलक में आनन्द-विभोर हुआ जा रहा हूँ कि तभी आया हवा का एक हलका झोंका और मेरी नाक पर मारा किसी ने तेज़ चाकू। नाक तो नहीं कटी, पर दिमाग़ भिन्ना गया। यह चाकू ख़ून करने वाला लोहे के फलक का चाकू न था, पेशाब की तेज़ दुर्गन्ध का चाकू था। बेंच की आड़ का लाभ उठाकर स्वतन्त्र भारत के नागरिक नर-नारियों ने इस स्थान का उपयोग किया था।
कुत्ते भी स्थान देखकर ही पेशाब करते हैं, पर उन नर-नारियों ने बिना स्थान देखे ही अपनी जरूरत पूरी की थी; क्योंकि इस बेंच से थोड़ी दूर पर ही सरकारी पेशाबघर था। मेरी इच्छा हुई कि मैं पूरे ज़ोर से रो पड़ूँ।
मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी और सामने ही सरकारी पेशाबघर था। मैं उधर मुड़ा, पर दरवाज़े तक अभी पहुँचा-न-पहुँचा कि तेज़ दुर्गन्ध का एक झोंका भीतर से आया। मसूरी की नगरपालिका इन दिनों सरकारी प्रबन्धक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) के हाथों में थी और मैं उनकी सफ़ाई-व्यवस्था का प्रशंसक था, पर इस झोंके की पहली ही झोंक में निन्दा का नशा मुझ पर छा गया-‘जाने कब से इस पेशाबघर में पानी की बूँद नहीं पड़ी। मज़ा आ जाए, अगर एक रात के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब को इसमें बन्द कर दिया जाए !’’
ज़रा आगे बढ़कर मैंने देखा कि भीतर पाँच मनुष्यों के लिए स्थान है और पाँचों स्थानों पर पाँच पढ़े-लिखे-सज्जन खड़े हैं। मैं बाहर लौटने को ही था कि देखा दूसरे पेशाबघरों की तरह यह भी प्रवाही (फ़्लश सिस्टम वाला) है और तीसरे स्थान के ऊपर वह साफ़ लगी है पानी की टंकी, जिसमें लटक रही है ज़ंजीर। इसमें नीचे एक छोटा कड़ा भी है कि उसमें दो उँगली डालें और दें ज़रा-सा झटका कि बस पाँचों स्थानों में बह जाए पानी ही पानी और दुर्गन्ध ऐसी भागे कि जैसे घरवालों के जागने पर चोर भागे।
मेरे पैर ठिठक गये। मैंने देखा, वे पाँचों सज्जन रूमालों से अपनी नाक दबाये खड़े हैं। क्या टंकी ख़राब है ? मेरे मन में नया प्रश्न उपजा कि मैंने आगे बढ़कर कड़े के द्वारा ज़ंजीर को ज़ोर का झटका दिया। पाँचों स्थानों के नल बादल की तरह बरस पड़े।
वे बरसे, मैं बाहर आया। मेरे पीछे ही पीछे एक दाढ़ी वाले सज्जन बाहर आये। उनकी पतलून के पाँवचे नीचे से भीग गये थे और बूटों में पानी आ गया था। मुझे उन्होंने कड़वी आँखों से घूरा कि इतने में वे चारों भी भीतर से बाहर आ गये। छींटे तो सभी पर तकड़े पड़े थे, पर शायद दाढ़ी वाले सज्जन दीवार से कुछ ज़्यादा सटकर खड़े थे, इसलिए उनकी पतलून पूरी तरह रसवर्षिणी हो गयी थी।
तमककर बोले-‘‘क्यों जी, यह आपने क्या हिमाक़त की ?’’ मैं इस समय स्वयं लड़ने की नहीं, तीतर लड़ाने की मूड में था। मुसकराकर मैंने कहा-‘‘हिमाक़त ? वह तो आपकी जान बचाने की हिकमत थी जनाब !’’
ग़ुर्राकर बोले-‘‘जान बचाने की कैसी हिकमत ?’’
मैंने अपने गले को पूरी तरह ठण्डा कर एक तेज़ आलपीन चुभाया-‘‘आप नाक को इतनी ज़ोर से दबा रहे थे कि मुझे आपका दम घुटने का ख़तरा दिखाई दिया; और भाई जी, यह तो बकरे भी जानते हैं कि दम घुटने से जान चली जाती है।’’
एक दूसरे साहब बीच में टमक पड़े-‘‘फिर आपको ज़ंजीर ही खींचनी थी, तो धीरे से खींचते। आपने तो ऐसा झटका मारा कि जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी हो।’’
बुजुर्गाना लहजे में मैंने कहा-‘‘हाँ, जी, मैंने यही समझा कि आप बड़ी मुसीबत में हैं।’’
वे समझ गये कि इस पत्थर पर जोंक नहीं लग सकती और खिसके। अपनी भीगी पतलून को एक झटका देते हुए वे सज्जन बोले-‘‘ऐसे-ऐसे जाहिल भी मसूरी आ जाते हैं.’’ मैंने उनकी व्यंग्य कविता को संगीत के जाहिल भी मसूरी आ जाते हैं।’’ मैंने उनकी व्यंग्य कविता को संगीत के स्वर में चढ़ाते हुए कहा-‘‘जी हाँ, यही तो बात है कि ऐसे-ऐसे जाहिल भी मसूरी आ जाते हैं कि बदबू में मरते रहते हैं, पर ज़ंजीर नहीं खींचते।’’
दिमाग़ में जोशीले लड़कपन का जो उबाल आया था, वह उतर गया, तो एक हलकी उदासी मुझ पर छा गयी-यों ही मैं उन बेचारों से उलझा; उनका या किन्ही दूसरों का इसमें कुछ भी दोष नहीं। उनसे पहले जाने कितने नागरिक आ चुके होंगे। वे सभी दुर्गन्ध के स्रष्टा थे, पर सभी उसके शिकार भी।
एक होता है नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है नागरिक का राष्टीय चरित्र। बेंच की आड़ में पेशाब करने वाले नर-नारी, नागरिक के चरित्र की दृष्टि से और राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से भी बुरे-से-बुरा नमूना थे; क्योंकि उनमें उचित स्थान देखकर ज़रूरत पूरी करने की नागरिक शालीनता भी नहीं थी और राष्ट्र के स्वच्छ-सुन्दर स्थानों को स्वच्छ-सुन्दर रखने की उदात्त राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था।
और सरकारी पेशाबघर के वे पाँच सज्जन ? वे कर्महीन थे, जिनमें राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाने की भी वृति नहीं थी, राष्ट्र को अपनी ओर से सुविधा देने की तो बात ही दूर। वे दो पैर के पशु थे, जो डण्डे से हँकते हैं, स्वयं सोच-विचारकर नहीं चलते।
प्रिंस क्रोपाटकिन का रूस के नये इतिहास में वही स्थान है, जो भारत को नये इतिहास में लोकमान्य तिलक का। रूस ज़ारशाही से मुक्त हो गया था और लेनिन महान् रूस की समाज-व्यवस्था को समाजवादी रूप देने में जुटे हुए थे। रूस के नागरिकों को नपा-तुला भोजन मिलता था और पूरे देश के दूध का पनीर बनाकर विदेशों को भेजा जाता था, जिसके बदले में मशीनें ख़रीदी जाती थीं। रूस के नागरिक दूध से वंचित थे। एक दिन लेनिन प्रिंस क्रोपाटनिक से मिलने गये। उनकी कमजोरी और बुढ़ापा देखकर लेनिन ने कहा-‘‘मैं आपके लिए एक गाय भेजने की विशेष व्यवस्था करता हूँ।’’
प्रिंस क्रोपाटकिन ने कहा-‘‘मैं भी रूस का एक नागरिक हूँ, इसलिए मैं अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं चाहता।’’ और कुछ दिन बाद प्रिंस क्रोपाटकिन की मृत्यु हो गयी।
दूसरे महायुद्ध के बाद जापान में भी राशनिंग करना पड़ा। सब नागरिकों को नपा-तुला अन्न मिलता था। एक रिटायर्ड जनरल की ख़ुराक ज़्यादा थी। राशनिंग में मिलने वाला अन्न कम पड़ता था, वे भूखे रह जाते थे। पास-पड़ोसियों ने उनसे कहा कि सरदार से ज़्यादा अन्न देने की प्रार्थना करें, पर उनका उत्तर था-‘‘युद्ध के कारण देश में अन्न की कमी है। सरकार व्यवस्था को सँभाल रही है, मैं सरकार का काम बढ़ाना नहीं चाहता। दूसरे नागरिक भी बहुत-सी दिक़्कतें बरदाश्त कर रहे हैं। मैं भी सबके साथ रहूँगा।’’ और रोज़-रोज़ की भूख से धीरे-धीरे उनकी मृत्यु हो गयी।
दूसरे महायुद्ध के बाद की ही बात है। इंग्लैण्ड टूटा-फूटा पड़ा था, हर चीज़ की कमी थी। भारत की अन्तरिम सरकार (1946-47) के मन्त्री जगजीवन राम जी किसी सम्मेलन में लन्दन गये। वहाँ की सरकार ने इधर-उधर जाने-आने के लिए एक टैक्सी दी और प्रेट्रोल के कूपन की एक कॉपी भी। पेट्रोल पर कण्ट्रोल था, पर इस सरकारी कूपन से कहीं भी, कितना भी लिया जा सकता था।
सम्मेलन के बाद मन्त्री जी जब भारत लौटने लगे, तो उस कॉपी में पाँच कूपन बाक़ी थे। टैक्सी के ड्राइवर से उन्होंने कहा-‘‘लो, ये कूपन तुम ले लो, तुम्हें इनसे लाभ होगा। अपनी टैक्सी के लिए पेट्रोल ले लेना।’’
मन्त्री जी का ख़याल था कि टैक्सी-ड्राइवर इससे ख़ुश होगा, उन्हें झुककर सलाम करेगा, पर वह तो सुनते ही गुस्से से भर गया-‘‘आप मुझे बेईमान समझते हैं ? मैं आपकी राय में गद्दार हूँ कि अपनी सरकार को धोखा देकर अपने लिए नियत भाग से अधिक पेट्रोल ले लूँगा ? आपके देश में ऐसे ही नागरिक होते हैं ? आप ये कूपन अपने स्वागत-अधिकारी को लौटाएँ; मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ ?’’
एक होता है नागरिक का अपना चरित्र और एक होता है नागरिक का राष्ट्रीय चरित्र। प्रिंस क्रोपाटकिन, जापानी जनरल और इंग्लैण्ड का ड्राइवर नागरिक के अपने और राष्ट्रीय चरित्र के उत्तम नमूने हैं। इसी श्रृंखला में ही जगजीवन राम का ही दूसरा संस्मरण है उसी यात्रा का। वे घुटनों में दर्द के कारण नाश्ते में अण्डा लेते हैं, पर द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन बम्बार्डमेण्ड से इंग्लैण्ड के मुर्ग़ीख़ाने क्षत-विक्षत हो गये थे, लन्दन में अण्डे पर कण्ट्रोल था; डॉक्टर के लिखने पर ही किसी को अण्डे मिलते थे। स्वागत-अधिकारी तीन दिन प्रयत्न करने पर भी जगजीवनराम जी को अण्डा नहीं दे सका। अन्त में उसने क्षमा-याचना की, तो जगजीवनराम जी ने पूछा-‘‘हाँ, आरम्भ में एक बार हुआ था। बात यह हुई कि डॉक्टर ने एक ग़रीब बीमार को दो दिन के लिए चार-चार अण्डे लिखे। वह मुर्ग़ीख़ाने से आठ अण्डे ले आया और अपने अमीर परिचित के हाथ काफ़ी ऊँचे मूल्य पर उन्हें बेच दिया। पता चलने पर पड़ोसियों ने इकट्ठे होकर उसका घर घेर लिया और उसकी इतनी निन्दा की कि उसे मुहल्ला छोड़कर भागना पड़ा, बस फिर कभी ऐसा नहीं हुआ।’’
आँख खोल देने वाले संस्मरण हैं ये और इनका सन्देश है कि यदि देश में किसी-किन्हीं चीज़ों की कमी हो, तो अच्छे चरित्र के नागरिक उसे धीरज से सहते हैं; सरकार को, समाज को अच्छी परिस्थितियाँ पैदा करने में सहयोग देते हैं, हुल्लड़ मचाकर, भ्रष्टाचार फैलाकर अव्यवस्था नहीं बढ़ाते। यही नहीं, यदि कोई चरित्रहीन नागरिक अपनी सुविधा या स्वार्थ के लिए अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करता है, तो राष्ट्रीय चरित्र के नागरिक सामूहिक रूप में उनका निन्दात्मक प्रतिवाद कर अव्यवस्था को असम्भव बना देते हैं।
राष्ट्रीय चरित्र अनुशासन से बनता है और अनुशासन की जड़ें नागरिकों के मन में जमती हैं राजदण्ड के भय से। धर्म भावना या प्रशिक्षण अनुशासन को सहज बनाकर उसे नागरिकों का स्वभाव-संस्कार बना देते हैं; इसे ही कहते हैं आत्मानुशासन। इस स्थिति में दण्ड-भय की कम-से-कम आवश्यकता रह जाती है। बीसवीं सदी के तीसरे दशक की बात है। हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में वरिष्ठ प्राध्यापक श्री गाँधी ने वार्षिक परीक्षा का प्रश्नपत्र तैयार किया और अपनी मेज़ के दराज़ में रख दिया। उनके पुत्र ने, जो उसी श्रेणी का छात्र था, वह पढ़ लिया और अपने दो मित्र-छात्रों को भी बता दिया। प्राध्यापक गाँधी को कुछ पता न चला। परीक्षा का परिणाम निकला, तो बेटे को 85 प्रतिशत अंक मिले।
वे चौंके, पुत्र से पूछा-‘‘तुम्हारे इतने नम्बर कैसे आये, सच बताओ !’’
बेटे ने बाप को रद्दा दिया-‘‘पापा, मैं रात में एक-एक बजे उठकर सुबह तक पढ़ा हूँ !’’ गाँधी अपने में स्पष्ट थे-‘‘वह सब मुझे मालूम है, तुम्हारे 65 प्रतिशत से अधिक नम्बर नहीं आ सकते; सच बताओ; नहीं तो भोजन नहीं करूँगा।’’ पुत्र ने स्वीकारा कि उसने प्रश्नपत्र देख लिया था और अपने दो साथियों को भी बताया है। प्रोफ़ेसर गाँधी ने उन साथियों के नाम नहीं पूछे और उसी दिन कुलपति पण्डित मदनमोहन मालवीय से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र का दो वर्ष के लिए वे ‘रस्टीकेशन’ (परीक्षा देने के अधिकार से वंचित) कर दें।
मालवीय जी बहुत दयालु थे। उन्होंने गाँधी को समझाया-‘‘प्रथम श्रेणी तो उसकी निश्चित थी ही, फिर उसने प्रश्नपत्र को बेचा नहीं, अपने दो मित्रों को ही बताया। अब यह रहने दो, बालक का भविष्य गड़बड़ा जाएगा।’’ गाँधी का उत्तर सदा स्मरणीय था-‘‘महाराज, मैं चुप रह जाऊँगा, तो हमारे विश्वविद्यालय की महिमा घटेगी’’ और वे आदेश पर हस्ताक्षर कराने के बाद ही उठे। प्रोफ़ेसर गाँधी आत्मानुशासन के उत्तम उदाहरण हैं। गाँधी जी अपने अहिंसात्मक युद्ध के द्वारा देश के जनमानस को आत्मानुशासन का सामूहिक प्रशिक्षण दे रहे थे, पर वह प्रक्रिया उनके बाद आगे नहीं बढ़ी। नागरिकों के लिए इसी प्रशिक्षण के निबन्धपुष्प खिले हैं अगले पन्नों में। इन संस्मरणात्मक निबन्धों में प्रचारक की हुंकार नहीं, सन्मित्र की पुचकार है, जो पाठक का कन्धा थपथपाकर उसे चिन्तन की राह पर ले आती है। वह सड़कों पर, स्टेशनों पर, दफ़्तरों में, घरों में ! कहें पूरे राष्टीय जीवन में कुरूपता देखता है और संकल्प करता है-मैं इस कुरूपता से बचूँगा और दूसरे नागरिकों को भी बचाऊँगा। बस प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए नागरिकों का कारवाँ तैयार हो जाता है। आगे का हर पन्ना उस कारवाँ के लिए हरी झण्डी है।
-कन्हैयालाल मिश्र
‘प्रभाकर’
मैं और मेरा घर
मैं जब लिखते-लिखते खिड़की से बाहर दाहिने
हाथ की तरफ़
झाँकता हूँ, तो एक ऊँचा मकान दिखाई देता है। कई मंजिलें हैं, जिनमें
छोटे-बड़े कमरे हैं, बरामदे हैं, स्नान-गृह हैं, शौचालय हैं इन कमरों में
पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, बालक हैं, हमेशा यहाँ रौनक़ रहती है। यह एक
होटल है।
मैं लिखते-लिखते जब अपनी खिड़की से बायें हाथ की तरफ़ झाँकता हूँ, तो एक ऊँचा मकान दिखाई देता है। कई मंज़िलें हैं, जिनमें छोटे-बड़े कमरे हैं, बरामदे हैं, स्नान-गृह हैं, शौचालय हैं। इन कमरों में पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, बालक हैं, हमेशा यहाँ चहल-पहल रहती है। यह एक धर्मशाला है।
मैं लिखते-लिखते अपनी खिड़की के पास बैठा अपने ही चारों ओर जब देखने लगता हूँ, तो देखता हूँ, यह है एक ऊँचा मकान। कई मंज़िलें हैं जिनमें कमरे हैं, बरामदे हैं, स्नान-गृह हैं, शौचालय हैं इन कमरों में पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं। यह एक घर है।
जाने कितने दिनों से मैं इस खिड़की के पास बैठकर लिखता हूँ, और न जाने कितनी बार इन तीनों मकानों पर मेरा ध्यान जा चुका है। पर उस दिन अचानक न जाने कहाँ से मन के आँगन में एक सवाल उभरकर खड़ा हो गया। ये तीन ऊँचे मकान ईंट-चूने की दीवारों से बने हैं, क़रीब-क़रीब एक ही तौर के हैं और इनमें वही स्त्री-पुरुष-बालक रहते हैं, फिर यह क्या बात है कि इनमें एक होटल है, एक धर्मशाला है और एक घर। तीनों में लोग रहते हैं, खाते-पीते हैं, जीवन का आनन्द लेते हैं, फिर ये तीनों ही घर क्यों नहीं हैं ?
आप जानते हैं, मेरी आदत सोचने की है, और यह आदत कोई फ़ालतू बात नहीं, यह सोचना ही मेरे जीवन की चरितार्थता है।
मैं लिखते-लिखते जब अपनी खिड़की से बायें हाथ की तरफ़ झाँकता हूँ, तो एक ऊँचा मकान दिखाई देता है। कई मंज़िलें हैं, जिनमें छोटे-बड़े कमरे हैं, बरामदे हैं, स्नान-गृह हैं, शौचालय हैं। इन कमरों में पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, बालक हैं, हमेशा यहाँ चहल-पहल रहती है। यह एक धर्मशाला है।
मैं लिखते-लिखते अपनी खिड़की के पास बैठा अपने ही चारों ओर जब देखने लगता हूँ, तो देखता हूँ, यह है एक ऊँचा मकान। कई मंज़िलें हैं जिनमें कमरे हैं, बरामदे हैं, स्नान-गृह हैं, शौचालय हैं इन कमरों में पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं। यह एक घर है।
जाने कितने दिनों से मैं इस खिड़की के पास बैठकर लिखता हूँ, और न जाने कितनी बार इन तीनों मकानों पर मेरा ध्यान जा चुका है। पर उस दिन अचानक न जाने कहाँ से मन के आँगन में एक सवाल उभरकर खड़ा हो गया। ये तीन ऊँचे मकान ईंट-चूने की दीवारों से बने हैं, क़रीब-क़रीब एक ही तौर के हैं और इनमें वही स्त्री-पुरुष-बालक रहते हैं, फिर यह क्या बात है कि इनमें एक होटल है, एक धर्मशाला है और एक घर। तीनों में लोग रहते हैं, खाते-पीते हैं, जीवन का आनन्द लेते हैं, फिर ये तीनों ही घर क्यों नहीं हैं ?
आप जानते हैं, मेरी आदत सोचने की है, और यह आदत कोई फ़ालतू बात नहीं, यह सोचना ही मेरे जीवन की चरितार्थता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i